प्राचीन भारत और खगोल विज्ञान- प्रसिद्ध जर्मन खगोलविज्ञानी कॉपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पूर्व आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गोल आकृति और इसके अपनी धुरी पर घूमने की पुष्टि कर दी थी। इसी तरह आइजक न्यूटन से 1000 वर्ष पूर्व ही ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त की पुष्टि कर दी थी। यह एक अलग बात है कि किन्हीं कारणों से इनका श्रेय पाश्चात्य वैज्ञानिकों को मिला।
इतिहास
भारतीय खगोल विज्ञान, जिसे ज्योतिष शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, का एक समृद्ध और जटिल इतिहास है जो 5000 साल से भी अधिक पुराना है। इसने भारतीय सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय खगोल विज्ञान के सबसे पुराने अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली-फूली।
वैदिक आर्य सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन गति से परिचित थे। वैदिककालीन खगोल विज्ञान का एक मात्र ग्रंथ ‘वेदांग ज्योतिष’ है। इसकी रचना ‘लगध’ नामक ऋषि ने ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व की थी। महाभारत में भी खगोल विज्ञान से संबंधित जानकारी मिलती है। महाभारत में चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण की चर्चा है। इस काल के लोगों को ज्ञात था कि ग्रहण केवल अमावस्या और पूर्णिमा को ही लग सकते हैं। इस काल के लोगों का ग्रहों के विषय में भी अच्छा ज्ञान था।
भारत में तारों के अध्ययन के सबसे पहले दर्ज संदर्भों में से एक ‘ऋग्वेद‘ में पाया जा सकता है, जो लगभग 2000 ईसा पूर्व के भजनों का संग्रह है। इन अभिलेखों से पता चलता है कि इस सभ्यता के लोगों को खगोल विज्ञान की बुनियादी समझ थी और वे तारों और ग्रहों की गतिविधियों का निरीक्षण करने में सक्षम।
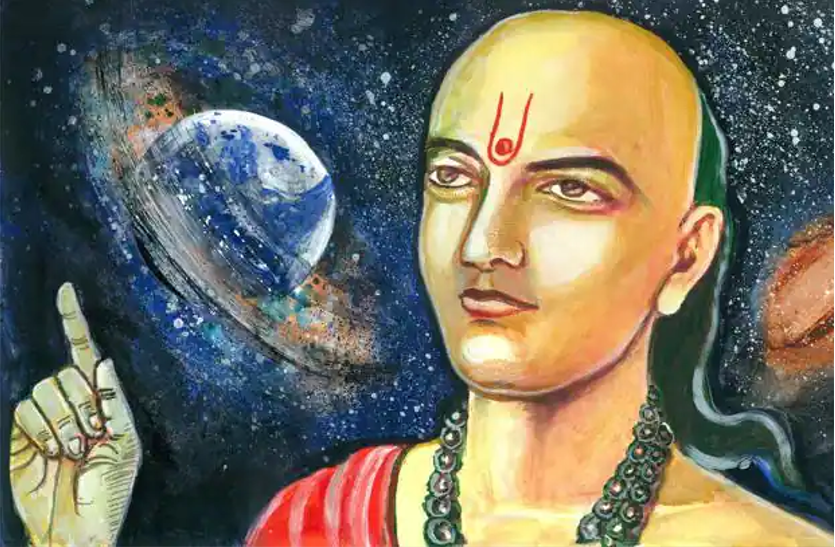
पाँचवीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम लोगों को बताया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। उन्होंने पृथ्वी के आकार, गति और परिधि का अनुमान भी लगाया था। आर्यभट्ट ने सूर्य और चंद्र ग्रहण के सही कारणों का पता लगाया। उनके अनुसार चंद्रमा और पृथ्वी की परछाई पड़ने से ग्रहण लगता है। चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। इसी प्रकार आर्यभट्ट ने राहु-केतु द्वारा सूर्य और चंद्र को ग्रस लेने के सिद्धान्त का खण्डन किया और ग्रहण का सही वैज्ञानिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया। आर्यभट्ट ने ‘आर्यभटीय’ तथा ‘आर्य सिद्धान्त’ नामक ग्रन्थों की रचना की थी।
छठी शताब्दी में वराहमिहिर नाम के खगोल वैज्ञानिक हुए। विज्ञान के इतिहास में वे प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने कहा कि कोई ऐसी शक्ति है, जो वस्तुओं को धरातल से बाँधे रखती है। आज इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। वराहमिहिर का कहना था कि पृथ्वी गोल है, जिसके धरातल पर पहाड़, नदियाँ, पेड़-पौधो, नगर आदि फैले हुए हैं। ‘पंचसिद्धान्तिका’ और ‘सूर्यसिद्धान्त’ उनकी खगोल विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकें हैं। इनके अतिरिक्त वराहमिहिर ने ‘वृहत्संहिता’ और ‘वृहज्जातक’ नाम की पुस्तकें भी लिखी हैं।
खगोल विज्ञान में भास्कराचार्य का विशिष्ट योगदान है। इनका समय बारहवीं शताब्दी था। वे गणित के प्रकाण्ड पण्डित थे। इन्होंने ‘सिद्धान्तशिरोमणि’ और ‘करण कुतुहल’ नामक दो ग्रन्थों की रचना की थी। खगोलविद् के रूप में भास्कराचार्य अपनी ‘तात्कालिक गति’ की अवधरणा के लिए प्रसिद्ध हैं। इससे खगोल वैज्ञानिकों को ग्रहों की गति का सही ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है।
निरीक्षण
ऋषि, या प्राचीन भारतीय ऋषि, अवलोकन, अंतर्ज्ञान और पौराणिक कहानियों के संयोजन के माध्यम से सितारों और खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम थे। वे आकाश का निरीक्षण करने, तारों और ग्रहों की गतिविधियों पर नज़र रखने और उनके द्वारा देखे गए किसी भी बदलाव या पैटर्न को नोट करने में घंटों बिताते थे।
प्राचीन भारतीय ऋषियों का मानना था कि ब्रह्मांड पांच तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश (या अंतरिक्ष)। उनका मानना था कि तारे और ग्रह ईथर से बने हैं, जो एक अदृश्य, भारहीन पदार्थ है जो ब्रह्मांड को भरता है। इस विश्वास ने उन्हें आकाशीय पिंडों की गतिविधियों की अत्यधिक सहज समझ विकसित करने की अनुमति दी।
प्राचीन ऋषियों ने तारों और ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कई पौराणिक कहानियों और ग्रंथों पर भी भरोसा किया था। उनका मानना था कि तारों और ग्रहों की गतिविधियाँ विभिन्न देवताओं और आध्यात्मिक शक्तियों से प्रभावित होती हैं, और आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को समझने के लिए इन शक्तियों को समझना आवश्यक है।
समय के साथ, प्राचीन ऋषियों ने समय मापने और तारों और ग्रहों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अत्यधिक सटीक तरीके विकसित किए। उन्होंने जटिल गणितीय सूत्र और खगोलीय तालिकाएँ विकसित कीं जिससे उन्हें बड़ी सटीकता के साथ आकाशीय पिंडों की स्थिति की भविष्यवाणी करने की अनुमति मिली।
समय के साथ, भारतीय खगोल विज्ञान एक अत्यधिक परिष्कृत विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। भारतीय खगोल विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक शून्य की अवधारणा का विकास था, जिसने अधिक सटीक खगोलीय गणना की अनुमति दी। भारतीय खगोलविदों ने समय मापने और आकाशीय पिंडों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अत्यधिक सटीक तरीके भी विकसित किए हैं।
योगदान
मध्यकाल के दौरान, भारतीय खगोल विज्ञान उपलब्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर द्वितीय जैसे विद्वानों ने त्रिकोणमिति के विकास और नई खगोलीय घटनाओं की खोज सहित क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
राजस्थान स्थित आमेर के राजा सवाई जयसिंह (द्वितीय) ने सन् 1733 में इस वेधशाला का निर्माण किया था। उस समय वे मालवा प्रांत के सूबेदार थे। उज्जैन के अलावा राजा जयसिंह ने दिल्ली, काशी, मथुरा और जयपुर में भी ऐसी ही वेधशालाओं का निर्माण किया। सबसे पहली वेधशाला बनी दिल्ली में, सन् 1724 में, जिसे जंतर मंतर कहा गया।

उन दिनों दिल्ली में मुगल बादशाह थे, मोहम्मद शाह। इनके समय हिन्दू और मुस्लिम खगोलशास्त्रियों के बीच कालगणना की सूक्ष्मता को लेकर बहस छिड़ी। तब भारतीय कालगणना की अचूकता को सिद्ध करने के लिए राजा जयसिंह ने इसे बनाया। इसका निर्माण होने के बाद जब यह पाया गया कि इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एकदम सटीक होता है, तब चार अन्य वेधशालाओं का भी निर्माण किया गया।
आधुनिक युग में भारतीय खगोलशास्त्र निरंतर फलता-फूलता रहा है। भारत कई विश्व स्तरीय वेधशालाओं का घर है, जिनमें हानले, लद्दाख में भारतीय खगोलीय वेधशाला और पुणे में विशाल मेट्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप शामिल हैं। भारतीय खगोलशास्त्री थर्टी मीटर टेलीस्कोप परियोजना सहित कई अंतरराष्ट्रीय सहयोगों में भी शामिल हैं।
आज, भारतीय खगोल विज्ञान एक अत्यधिक अंतःविषय क्षेत्र है जो भौतिकी, गणित, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के तत्वों को जोड़ता है। भारतीय खगोलशास्त्री कई प्रकार की अनुसंधान परियोजनाओं में शामिल हैं, जिनमें एक्सोप्लैनेट, ब्लैक होल और आकाशगंगाओं के विकास का अध्ययन शामिल है।
यहां इसके कुछ प्रमुख निष्कर्ष और महत्व दिए गए हैं:
समय और कैलेंडर की गणना: भारतीय खगोलविदों ने समय की गणना के लिए परिष्कृत गणितीय प्रणालियाँ विकसित कीं, जिनका उपयोग धार्मिक और कृषि उद्देश्यों के लिए कैलेंडर बनाने के लिए किया गया था। भारतीय कैलेंडर चंद्रमा की स्थिति पर आधारित है और आज भी उपयोग में है।
आकाशीय पिंडों का अवलोकन: भारतीय खगोलविदों ने तारों, ग्रहों और धूमकेतुओं जैसे आकाशीय पिंडों का विस्तृत अवलोकन किया। उन्होंने इन वस्तुओं की गति को भी रिकॉर्ड किया और उनके व्यवहार को समझाने के लिए गणितीय मॉडल विकसित किए।
ज्योतिष: भारतीय खगोल विज्ञान ज्योतिष से निकटता से जुड़ा हुआ है, और दोनों का अभ्यास अक्सर एक साथ किया जाता है। माना जाता है कि भारतीय ज्योतिष किसी व्यक्ति के जन्म के समय आकाशीय पिंडों की स्थिति के आधार पर उसके व्यक्तित्व, भाग्य और रिश्तों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
गणित में योगदान: भारतीय खगोलविदों ने गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें दशमलव प्रणाली का विकास और शून्य की अवधारणा का आविष्कार शामिल है।
सांस्कृतिक महत्व: खगोल विज्ञान ने कला, साहित्य और धर्म को प्रभावित करते हुए भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, हिंदू पौराणिक कथाओं में सितारों और ग्रहों के बारे में कई कहानियां हैं, और कई त्योहार खगोलीय घटनाओं के आधार पर मनाए जाते हैं।
संक्षेप में, भारतीय खगोल विज्ञान का भारतीय सभ्यता के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, और इसके निष्कर्षों का आज भी अध्ययन और जश्न मनाया जाता है। भारत के ऋषि अवलोकन, अंतर्ज्ञान और पौराणिक कहानियों के संयोजन के माध्यम से सितारों और खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम थे। उन्होंने समय मापने और आकाशीय पिंडों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अत्यधिक सटीक तरीके विकसित किए, जिससे उन्हें खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने की अनुमति मिली।
मंदिर और उपनिवेशवाद का विनाश – संप्रभुता की गूँज बिखर गई – अध्याय 2



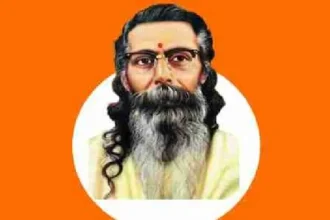


 If you want to use your preferred UPI app, our UPI ID is raj0nly@UPI (you can also scan the QR Code below to make a payment to this ID.
If you want to use your preferred UPI app, our UPI ID is raj0nly@UPI (you can also scan the QR Code below to make a payment to this ID.






